मैथिली का मांगल गीत

(वेद विलास उनियाल वरिष्ठ पत्रकार)
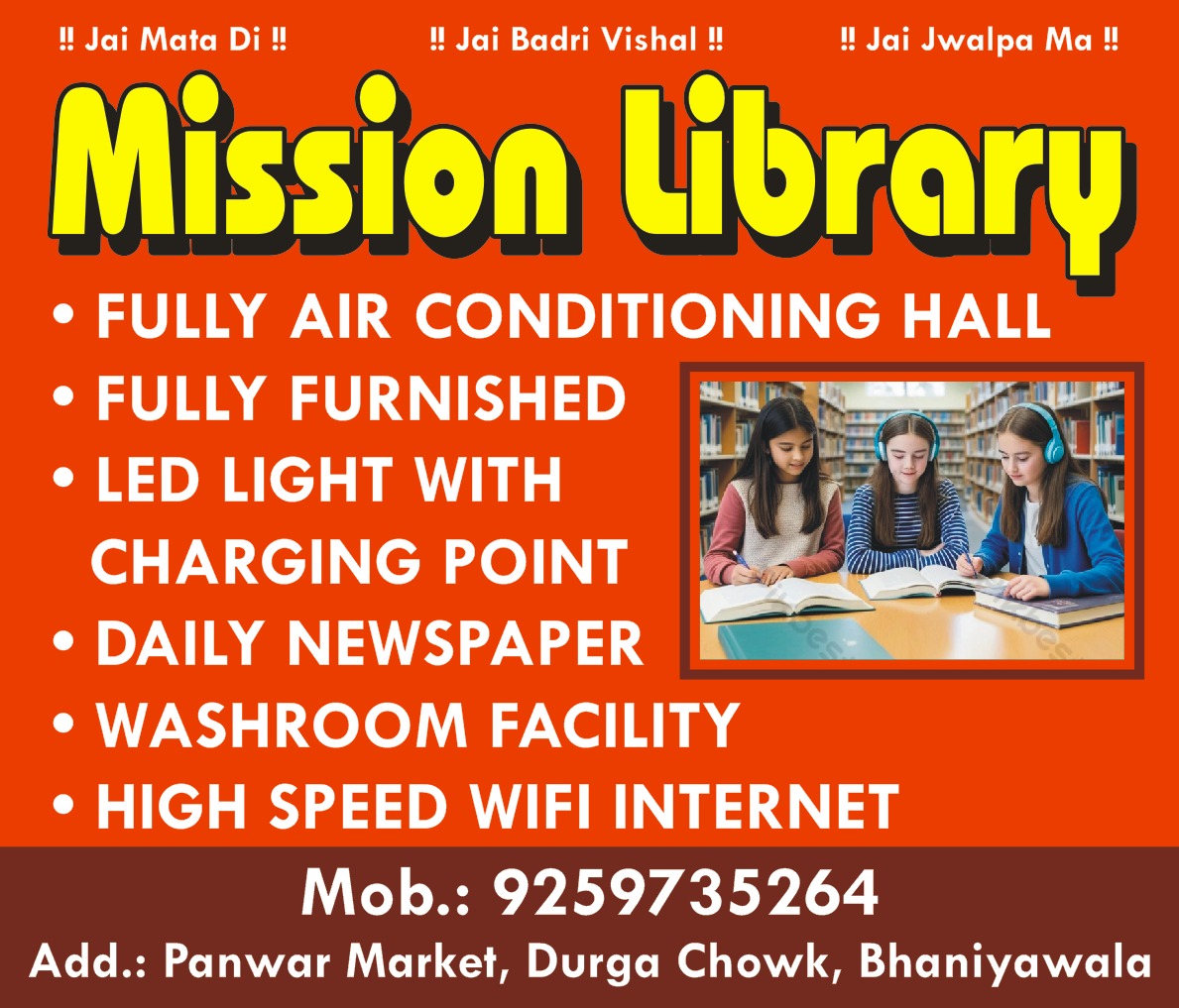
यही लोकसंगीत का ओज और मार्धुय हैं कि मधुबनी की मैथिली उत्तराखड के मांगल और शुभ गीतों का गाती है और यहां का जनमानस उसमें झूमने लगता है। लोकसंगीत लोकजीवन से आता है। और हर क्षेत्र इलाके के अपनी पंरपरा जीवन शैली थोडी भिन्ह जरूर हो सकती है लेकिन उसका भाव एक ही होता है, लोकजीवन कहीं का भी हो एक सा ही झंकृत होता है। इसलिए भाषा कुछ अलग हो सकती है लेकिन उनके भाव रस समान होता है। इसलिए मैथिली भोजपुरी हो उत्तराखंडी या छत्तीसगढी इनके लोकजीवन से निकले गीत अपना प्रभाव छोड़ते हैं। आप बुंदेलखंडी गीतों को सुनिए या हिमाचली आपको गीतों का सार एक सा लगेगा। छठ के गीतों में सूर्य की आराधना का जो भाव ह उत्तराखंड में उसी तरह की लोकध्वनि मकरसंक्रांति पर्व से जुड़े गीतों में मिलती है । वही असम के बिहू गीतों में भी झलकता है। उत्तराखंड के मांगल गीतों को सुनिए और फिर अवध के सीता विवाह के प्रासंगिक गीतों को सुनिए वही कसक महसूस होगी। ऐसा ही कुछ पंजाब की हीर गीतो में सुनाई देता है। बिहार में बेटी की विदाई के समय गाया जाने वाला समदाउन गीत इसी तरह का अहसास लिए है।

(देखिए पूरी वीडियो…..)
कहीं न कहीं उस भाव को मैथिली ने भी अपने मधुबनी क्षेत्र में उस भाव को महसूस किया । इसी लिए जब उसने उत्तराखडी मांगल के स्वर पकडे तो उसे पूरी शुद्धता तक ही नहीं ले गई बल्कि अपनी प्रस्तुति मे पूरी तरह तन मन से डूब गई। यही भारत की विविधता का स्वरूप है और यही यहां के लोकरंग की पहचान है। थोड़ा थोड़ा अलग होकर भी यहां की संस्कृति मिली जुली है उसमें एक तरह की समरसता की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है।
जब कलाकार स्वरों को साध लेता है और गायक में निपुणता आ जाती है तो गीत किसी भी भाषा का हो उसे एक स्तर तक पहुंचा देता है। ऐसे में समाज की कलाकार को सराहना मिलती है कि उसने दूसरी भाषा बोली का गीत को गाया। लेकिन इसका खास पहलू यह है कि किसी ऐसे आंचलिक या क्षेत्रीय गीत को गाते हुए या किसी नृत्य को करते हुए उसे किस स्तर तक महसूस किया गया। मैथिली ने जब सुभ कागा या विवाह का मांगल गीत गाने के लिए चुना तो उसे पहले गहरे गहरे आत्मसात किया। उसने मांगलों की उन परंपरा उसका रिवाज संगीत और उसमें उसमे समाहित भाव को समझा। बिना जाने समझे केवल शब्दों को पंक्तिबद्ध गाती तो सुर निश्चित सुरीला होता पर उसमें अलोकिक भाव नहीं होता। मैथिली ने अगर केवल सोशल मीडिया को ध्यान में रखकर गाया होता तो यह ऐसा गायन होता जो कुछ दिन सुना जाता फिर ओझल हो जाता। लेकिन केवल स्वर बल्कि जो वीडियो आया है उसमे उसकी भावभंगिमा को देखिए तो अहसास हो जाता है कि गाने में पूरी तन्यमता से डूबी है। यह किसी स्टेज शो के लिए खास तौर पर तैयार किया गायन नही था। बल्कि इसके पीछे यही कोशिश थी कि देश की लोकसंस्कृतिक आंचलिकता के विराट अस्तित्व को समझते हुए जो सुंदर है उसे बाहर लाया जाए। निश्चित उत्तराखंड के लोक मांगल गीतों को दशकों से कलाकार गाते रहे हैं लेकिन दूर मिथिला की एक लडकी इसे गुनगुनाए गाए तो यह साधूवाद है। मैथिली ने किसी लोक फिल्म या टीवी सीरियल के लिए नहीं गाया। गायिका मैथिली ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल पर इस गीत के वीडियो को रिलीज किया है। इसमें उसके भाई ऋषभ व अयाची भी वाद्य यंत्रों पर संगत दे रहे हैं। मैथिली ने पहले कुमांउनी मांगल गीत सुवा ओ सुवा बनखंडी सुवा.. को गाकर खूब चर्चा बटोरी थी। अब मैथिली का हल्दी हाथ गढ़वाली लोक गीत दे द्यावा बाबाजी, गौ कन्या दान गीत सुना जा रहा है। मैथिली कुछ समय पहले एक कार्यक्रम में देहरादून डोइवाला आई थीं । यहां उन्होंने उत्तराखड के लोकगीतों को सुना और उत्तराखंडियों के लोकसंगीत के प्रति गहरी ललक को महसूस किया। संभव है उसी समय उन्होंने उत्तराखंड के गीतों को गाने का मन बना लिया हो।
कला संगीत की यही व्यापकता है। हम इस बात पर खुश हो सकते हैं कि कोई बाहरी राज्य का कलाकार हमारी बोली भाषा काकोई गीत संगीत अपना रहा है। लेकिन यही कोशिश हमारे अपने स्तर पर भी होनी चाहिए । हम अपने उत्तराखंड के लोकगीत संगत पर शोध करे उसे और पल्लवित करें लेकिन साथ ही साथ दूसरी लोकसंस्कृतियों को भी जाने समझे। ले देकर हम पंजाब के आधुनिक गीत संगीत को अपना लेते हैं। बृज बुंदेलखंडी छत्तीसगढी भोजपुरी मिथिला असमी मणिपुरी गुजराती आदि के विराट सांस्कृतिक भाव तक जा पाएं तो पूरे भारतीय परिवेश को महसूस करेंगे। कहना होगा कि मैथिली ठाकुर और उसके भाइयों की ऐसी पहल एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति के लिए दरवाजे खुलने जैसा है। उत्तराखंड ने अपनी लोकसंस्कृति परंपरा से जो गीत संगीत पाया है वैसा ही बिहार ने छठ बंगाल ने नवरात्री में पाया है। उत्तराखंड बासंती गीतों में जिस तरह इठलाता झूमता है असम का बिहु भी वैसा ही खिलखिलाता हुआ नजर आता है। लोकजीवन आंचलिक ग्रामीण परिवेशों से निकली चीजें अपना बोध कराती है। लोकजीवन से ही झूमर चैती फागू कजली बारहमासा निकले है। इनमें लय है मिठास है। जीवन के सुंदर रंग है। जीवन की अनूभूति है और सुख दुख है।
फिल्मों के गीत संगीत में यह साफ दिखा है। आचंलिक या कस्वाई ग्रामीण परिवेश से निकले गीत लोगों की जुबान पर रहे हैं। महसूस किया जा सकता है कि राजकपूर के पास गीत संगीत का खजाना था लेकिन बेटी की शादी के वक्त के लिए उन्होने पंजाबी हीर तैयार करवाई थी। माटी की वही सुंगध हमें उत्तराखंड के मांगल गीतों की ओर ले जाती है। डीजे के शोर शराबों के बीच कुछ पल के लिए सही मांगल गीत कहीं सुनाई दें तो उसका अहसास अलग झलकता है। यह हमारी धरोहर है। लोकमंगल की कामना करने वाले गुमनाम सिद्ध कलाकारों ने जब मांगल गीतों को रचा होगा उनका संगीत सृजन किया होगा वह अनूठा अलौकिक अवसर रहा होगा।
गढ़वाल क्षेत्र में वैवाहिक रस्म में हल्दी हाथ के दौरान मांगल गीत को गाने की पुरानी परंपरा रही है। इस मांगल गीत में कन्या दान को सभी दानों में श्रेष्ठ और अनूठा दान माना गया है।
किसी दैवीय भाव में लीन रहकर ही ऐसी विधाएं सामने आई होंगी। गहरे साधकों ने मांगल शुभ गीतों को रचा होगा। इसलिए आज उन गीतो पहाडों की रेखा धस्माना गाए, हेमा करासी गाए या मैथिली भूमि की मैथिली ठाकुर उनका संदेश दूर तक जाता है। शायद यही कहता हुआ कि अपनी इस विराट सांस्कृतिक विरासत से दूर न जाए। बात केवल मांगलगीतों की नहीं पूरे लोकजीवन से जुडे गीतों की है।
जिस बिहार की भूमि में बिंदेश्वरी देवी मुन्नी जी शारदा सिन्हा जैसी गयिका हुई हैं वही मैथिली ठाकुर एक नई बडी संभावनाओं के साथ है। मैथिली जिस भूमि से हैं वह श्रंगार और रस के महाकवि विद्यापति की भूमि है। मिथिलांचल में लोककला लोकउत्सव का जीवन है। यहीं से देवभूमि का लोकमांगलिक गीत मंद हवाओ की तरह हम तक पहुंचा है। इसका स्वागत करना चाहिए। उत्तराखंड के लोगो का आभार मैथिली ठाकुर को और प्रेरित करेगा। पुराने लोकगीत लोकसंगीत को उत्तराखंड के कलाकार भी दोहराते रहे हैं। लेकिन मैथिली का उसे दोहराना गाना कुछ अलग मायने रखता है।

Explore the ranked best online casinos of 2025. Compare bonuses, game selections, and trustworthiness of top platforms for secure and rewarding gameplaycasino bonus.