जब हम उद्यान विकास की बात करते हैं उसके अंतर्गत फल उत्पादन, सब्जी एवं सब्जी बीज उत्पादन, फूलों की खेती, मसाला फसलों की खेती , मशरूम उत्पादन, औषधीय व सगन्धीय फसलों की खेती , मधुमक्खी पालन , जैविक खेती आदि विषय आते हैं इन बिषयो को अपना कर घर पर ही स्वरोजगार कर आर्थिक विकास कर सकते हैं।

उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल हिमालय की तराई से लेकर बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों तक फैला हुआ है, जिसके कारण प्रदेश की जलवायु में अत्यधिक विविधता पाई जाती है,जो सभी प्रकार के कृषि एवं बागवानी फसलों के लिए अनुकूल है। बागवानी विकास से राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की जा सकती है।
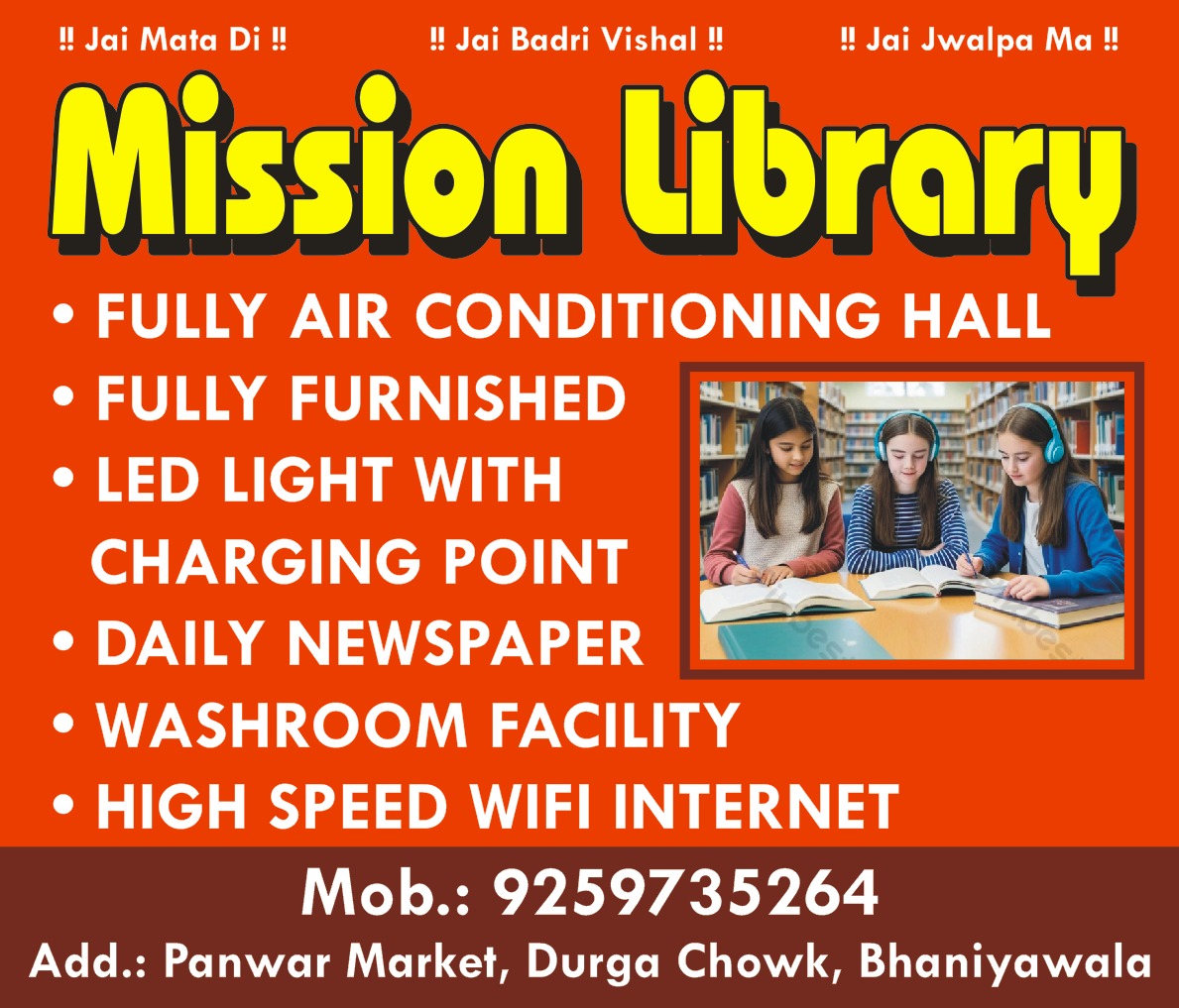
राज्य में उद्यान विकास हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखंड लगातार सतत् प्रयास कर रहा है। गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विशव विद्यालय पन्त नगर एवं औद्यानिकी महाविद्यालय,भरसार पौड़ी गढ़वाल बागवानी अनुसंधान एवं प्रसार की आधुनिक विकास की दिशा कार्यरत हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,नई दिल्ली एवं गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के सहयोग से प्रदेश के 13 जनपदों में कृषकों को वैज्ञानिक /तकनीकी जानकारी देने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केन्द्रौं की स्थापना की गई है।
राज्य में उद्यान विकास हेतु जिला योजना, राज्य सैक्टर की योजनाएं, केन्द्र पोषित एवं वाह्य सहायतित कई योजनाएं चलाई जा रही है।
प्रमुख गतिमान योजनाएं-
पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन की योजना।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य औद्यानिक फसलौं का कल्सटर मैं उत्पादन कर स्थानीय कृषकों को आर्थिक रूप से सुद्रिण करना है । योजना के अन्तर्गत कृषकों से उन्नत किस्मौं के फल पौध, मसाला विकास एवं सव्जी बीजौं का उत्पादन करवाकर आत्म निर्भर बनाना है। 2003-04 से यह योजना संचालित की जा रही है जिसपर अब तक सात सौ ( रूपये 700) करोड़ से भी अधिक का व्यय किया जा चुका है।
प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के प्रति बूंद अधिक फसल घटक, केंद्रीय प्रायोजित योजना सूक्ष्म सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएमआई) को 2011-12 के वर्ष में उत्तराखंड राज्य में सिंचाई की उन्नत पद्धति के तहत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। बागवानी और कृषि विकास के लिए प्रोत्साहन। 2014-15 से इस योजना को सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत कृषि जल प्रबंधन के नाम से विलय कर दिया गया है। योजना के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) : जैविक खेती को बढ़ावा देने का उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के मिश्रण के माध्यम से दीर्घकालिक मिट्टी की उर्वरता निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए जैविक खेती के टिकाऊ मॉडल का विकास करना है।
फसल बीमा योजना: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बागवानी फसलों के लिए पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत 13 बागवानी फसलें (सेब, आड़ू, माल्टा, मौसंबी, संतरा, आम, लीची, आलू, अदरक, टमाटर, मटर, फ्रेंच बीन्स और मिर्च) निर्धारित हैं।
सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएम एफएमई) का प्रधान मंत्री औपचारिककरण:
माननीय प्रधान मंत्री द्वारा घोषित “आत्म निर्भर भारत अभियान” के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत व्यक्तिगत, स्वयं सहायता समूह और एफपीओ को सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के लिए 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
ऑपरेशन ग्रीन स्कीम्स ( टॉप टू टोटल) : यह किसानों को उपभोक्ताओं से जोड़कर टमाटर, प्याज और आलू (टॉप सब्जियों) के संगठित विपणन पर केंद्रित है।
बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना
जापान इंटरनेशनल को-आपरेशन एजेंसी (जायका) ने 540 करोड़ रुपये की लागत से उत्तराखंड एकीकृत औद्यानिकी विकास परियोजना स्वीकृति है। जायका से राज्य के चार जिलों टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल व पिथौरागढ़ में परियोजना संचालित की जाएगी। इसके अंतर्गत सेब, अखरोट व कीवी फलों के सेंटर आफ एक्सीलेंस भी स्थापित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना –
राज्य के युवाओं को रोजगार देने एवं कृषकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत उद्यान विभाग प्रत्येक जनपद में 90% अनुदान पर पालीहाउस लगवा रहा है। योजना में 1219 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 100 वर्ग मीटर पौलीहाउस के निर्माण पर 121900 ( एक लाख इक्कीस हजार नौ सौ ) रुपए की लागत आती है जिसमें कृषक को 12190 रुपए का भुगतान करना होता है।
एपिल मिशन योजना।
पर्वतीय जनपदों में सेब के अति सघन उद्यानों की स्थापना हेतु यह योजना संचालित की गई है। योजनान्तर्गत प्रति बागान 0.40 है० (याने 20 नाली) हेतु कुल निर्धारित लागत अधिकतम रुपए 12 लाख का 80% याने 9.60 लाख प्रति लाभार्थी की दर से सब्सिडी के रूप में राज्य सहायता प्रदान की जायेगी।
मुख्यमंत्री एकीकृत बगवानी विकास योजना:- मुख्यमंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में उद्यानिकी के अन्तर्गत रिवर्स पलायन के प्रबन्धन हेतु कोविड-19 महामारी के प्रभाव के दौरान प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के तहत इनपुट अर्थात सब्जी के बीज, फल के पौधे, फूल के बीज/पौधे, कीटनाशक, जैव कीटनाशक आदि का प्रावधान 50-60% की सीमा के साथ किया गया था।
मधुग्राम : निर्णय लिया गया कि मधुमक्खी पालन क्लस्टर आधार पर किया जायेगा. इस संबंध में किसानों, बेरोजगार युवाओं और भूमिहीन किसानों के लिए राज्य की प्रत्येक नया पंचायत में एक मधुग्राम स्थापित किया जाएगा।
जनपद स्तर पर एक जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय तथा ब्लाक/न्यायपंचायत स्तर पर उत्तराखंड के समस्त जनपदों में 186 उद्यान सचल दल केन्द्रौं के माध्यम से उद्यान विभाग की यौजनाऔं का संचालन किया जाता है।
पहाड़ी क्षेत्रों में जोत का आकार कम व विखरा होना, चक्कवन्दी का न होना, बर्षा आधारित खेती, जंगली जानवरों सुवर बन्दर से फसलों को नुक़सान, प्राकृतिक आपदाओं (जैसे अतिवृष्टि,ओला वृष्टि , वे मौसम बरसात, अधिक ठंड व पाला आदि) से फसलों को होने वाले नुक़सान,गुणवत्ता युक्त फसल निवेशों (फल पौध,बीज,दवा,खाद आदि) की कमी एवं समय पर न उपलब्ध होना, आधुनिक तकनीकों के प्रचार प्रसार में कमी, ढांचा गत एवं परिवहन सुविधाओं का अभाव,विपणन में विचौलियों का बाहुल्य, भंडारण एवं प्रसंस्करण सुविधाओं का अभाव, तुड़ाई उपरान्त प्रबंधन सुविधाओं का न होना, अनुसंधान विकास एवं प्रसार क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों एवं कृषकों में समुचित समन्वय का अभाव , योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता का न होना आदि कई समस्याएं हैं जिस कारण पहाड़ी जनपदों में अपेक्षित उद्यान विकास नहीं हो पा रहा है।
पहाड़ी क्षेत्रों में उद्यान विकास की अपार संभावनाएं हैं यहां आलू अदरक,प्याज, लहसुन, मसाला मिर्च की व्यवसायिक फसलें परंपरागत रूप से उगाई जाती आ रही है योजनाओं से किसानों की मदद कर इन फसलों के उन्नत किस्म के बीज कृषि विश्वविद्यालयों से मंगा कर कृषकों से इन व्यवसायिक फसलों के बीज उत्पादन कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास होने चाहिए।
पहाड़ी क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन का अपना विशेष महत्व है। जिस समय मैदान क्षेत्रों में सब्जियों का उत्पादन नहीं हो पाता तथा अभाव रहता है उस समय (गर्मी व बर्षात ) पहाड़ी क्षेत्रों में सब्जियों (मटर बन्दगोभी, फूल गोभी, टमाटर,सिमला मिर्च,खीरा,फ्रासवीन,मूली,हरा धनिया आदि ) का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है इस प्रकार बेमौसम में सब्जियां का उत्पादन कर यहां का कास्तकार अच्छा आर्थिक लाभ अर्जित कर सकता है।
पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादित सब्जियां अधिक स्वादिष्ट पौष्टिक शुद्ध व रसायन मुक्त होती है। यूरोपीयन सब्जियां (ब्रोकली,ब्रुसल स्प्राउट्स,रेड कैवैज,आर्टीचोक,लैट्यूस आदि) का उत्पादन पर्वतीय क्षेत्रों में आसानी से किया जा सकता है।
सब्जी व्यवसाय में उत्पादन से लेकर वितरण तक अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।
बन्द गोभी फूल गोभी,गाजर,मूली, चुकुन्दर आदि सब्जियों के बीज उत्पादन की अपार संभावनाएं है।
उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री एवं यमुनेत्री धाम तथा कई पर्यटक स्थल होने के कारण माह मई से लेकर सितंबर तक लाखों यात्री एवं पर्यटक राज्य के भ्रमण पर आते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में आड़ू, प्लम, खुबानी से माह मई से अगस्त तक फल प्राप्त होते हैं,यात्रा मार्ग के स्थानों में इन फलों का उत्पादन कराया जा सकता है जिससे उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों एवं पर्यटकों को फल उपलब्ध हो सकें इससे स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।
पहाड़ी क्षेत्रों के कृषक परंपरागत रूप से जैविक खेती करते आ रहे हैं,इन क्षेत्रों के कृषकों द्वारा कृषि कार्यों में रसायनिक उर्वरकों तथा दवाओं का उपयोग कम मात्रा में किया जाता है। स्थानीय उपलव्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए स्थानीय वेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर तथा सीमांत एवं लघु सीमांत गरीब कृषकों की उपज को जैविक मोड़ में ला कर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारी जा सकती है।
जैविक खेती कर उत्तराखंड को कृषि आधारित, प्रदूषण मुक्त, स्वास्थ्य वर्धक एवं स्वावलंबी राज्य बनाने की ओर अग्रसर किया जा सकता है।
पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक तापक्रम में ऊंचाई के हिसाब से बटन मशरूम बर्ष भर में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चार, मध्य में तीन एवं घाटी वाले क्षेत्रों में दो बार उत्पादन लिया जा सकता है। प्राकृतिक तापक्रम में मशरूम उत्पादन में लागत काफी कम आती है वहीं दूसरी ओर मैदानी क्षेत्रों में मशरूम उत्पादन हेतु नियंत्रित तापक्रम की आवश्यकता होती है जिस कारण इन क्षेत्रों में मशरूम उत्पादन पर लागत अधिक आती है।
समय पर स्पान ( मशरूम बीज) व खाद उपलब्ध कराकर युवाओं को मशरूम उत्पादन से जोड़ कर स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है।
भौगौलिक परिस्थिति एवं जलवायु में विविधता होने के कारण उत्तराखंड राज्य में बागवानी विकास के अन्तर्गत फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, फूलों की खेती, मसाला व सब्जी बीज उत्पादन, मशरूम उत्पादन, औषधीय व सगन्धीय फसलों की खेती एवं मधुमक्खी पालन जैविक खेती आदि की अपार संभावनाएं हैं। जबतक क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति के अनुसार योजनाओं में सुधार नहीं किया जाता तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता नहीं लाई जाती राज्य में अपेक्षित उद्यान विकास होगा सोचना बेमानी है।
Explore the ranked best online casinos of 2025. Compare bonuses, game selections, and trustworthiness of top platforms for secure and rewarding gameplaycasino.